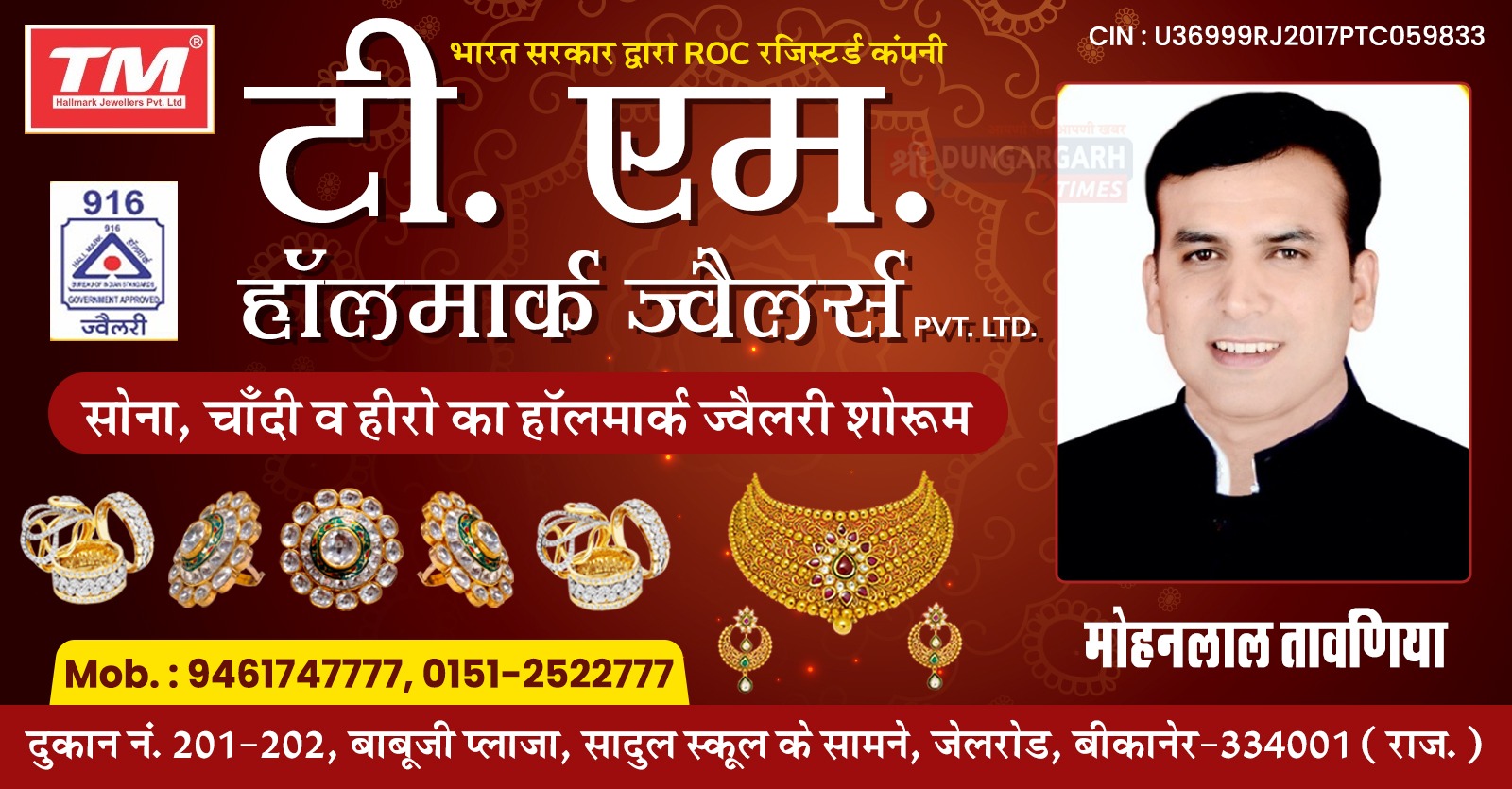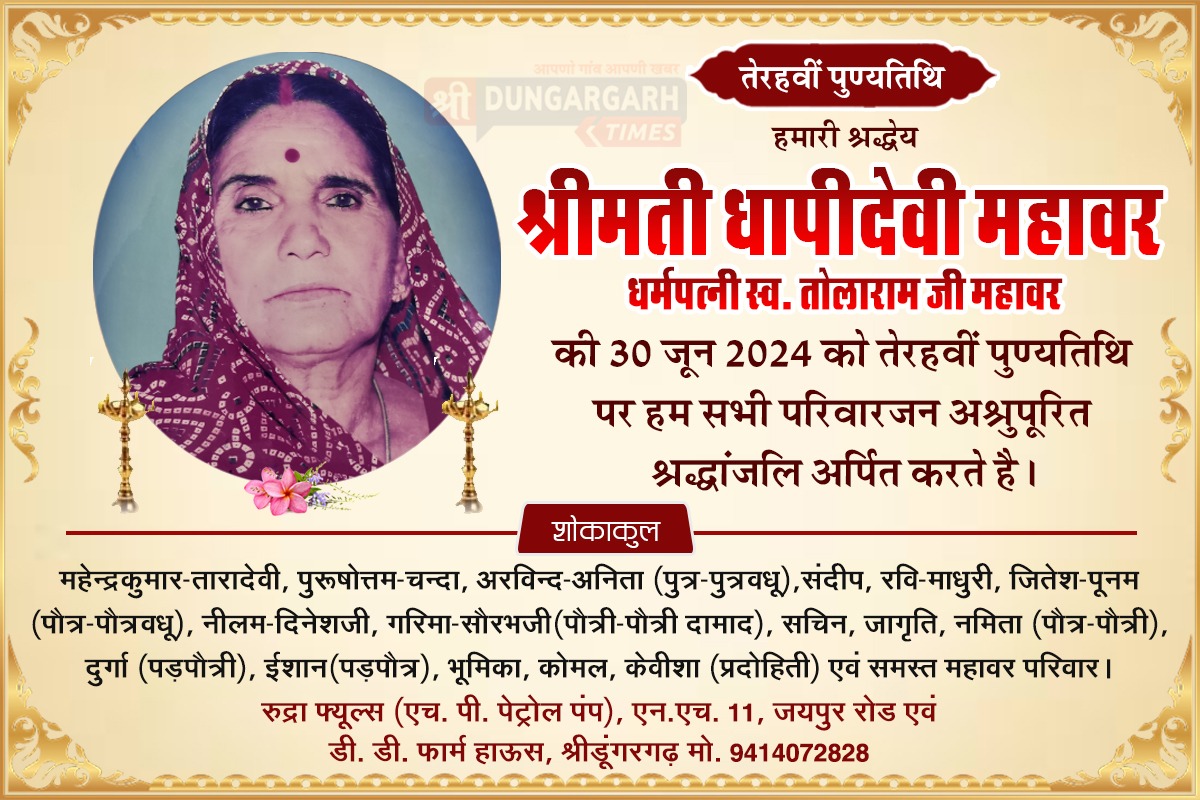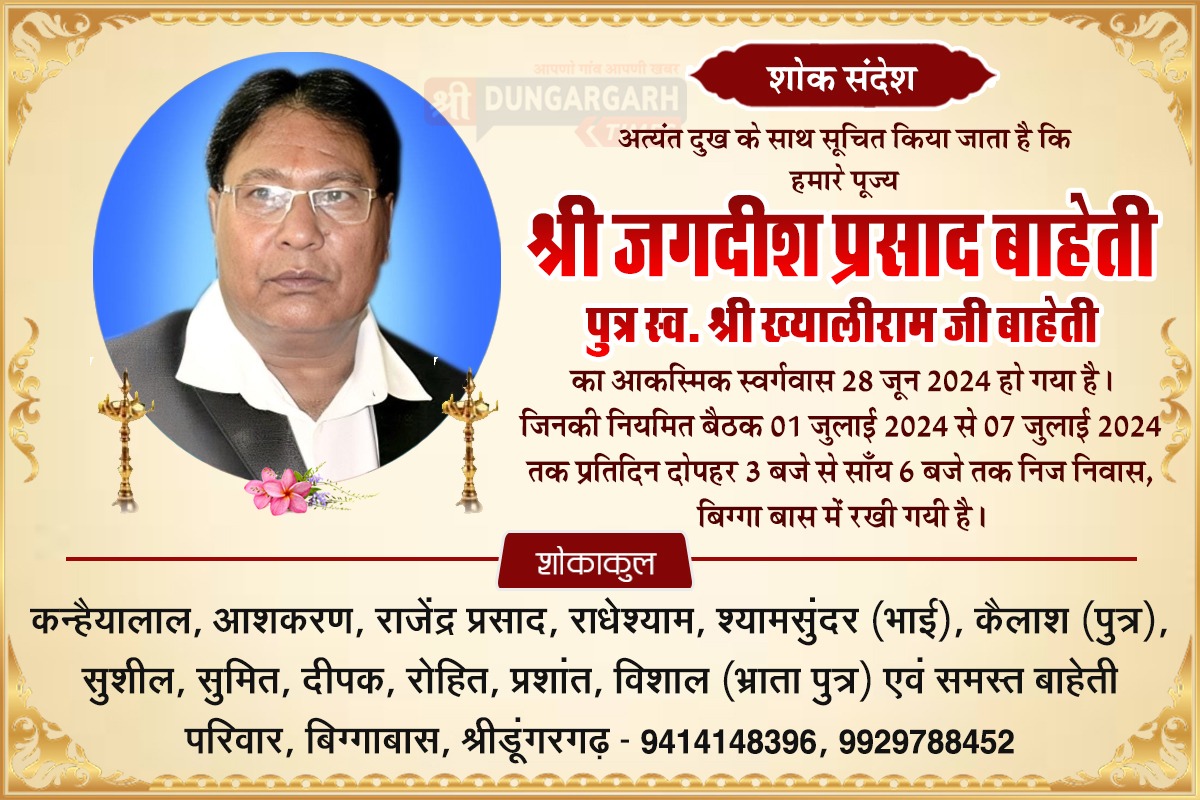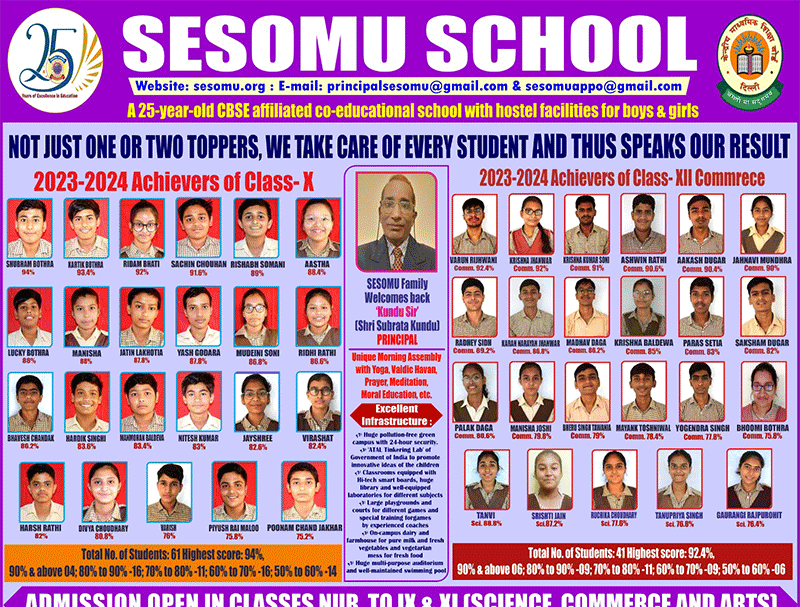


श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 25 जून 2024। ” राष्ट्रीय आपातकाल” का नाम सुनते ही सर्वप्रथम किसी भी चिंतनशील व्यक्ति के मस्तिष्क में क्या आता है? मेरे विचार से हम में से अधिकांश को देश की तत्कालीन विकट परिस्थितियों की स्मृति होगी जिसमें बदहाल कानून व्यवस्था, शोषण और दमन से भरी नीतियों के दम पर लोगों को मजबूर करके सरकार द्वारा अपनी बात मनवाने के चित्र जेहन में उभरते है, आप तनाव, डर और जोर जबरदस्ती के माहौल के बारे में भी याद करेंगे, परंतु कल्पना कीजिये की हमारी पूर्वव्रर्ती पीढ़ियों ने आपातकाल के भयानक समय का सामना किस तरह किया होगा.? ठहरिए, जब भी राष्ट्रीय आपातकाल का जिक्र होता है तो केवल मस्तिष्क में पूर्व प्रधानमंत्री का नाम ही गूंज उठता है। ये इसलिए, क्योंकि इंदिरा गांधी द्वारा अचानक और रहस्यमयी तरीके से लिए गए इस एक फैसले ने देश के सामाजिक व आर्थिक ताने-बाने की बुनियादें हिला दी। 1975 का आपातकाल इतिहास में काले दौर के रूप में अंकित है। ये समय अनिश्चितता, भ्रम और तनाव का समय था। आप ये जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आजकल कुछ राजनीतिक लोग उस समय का महिमामंडन स्वर्णयुग की तरह कर लोगों को बरगलाने का प्रयास कर रहें है। आज के समय को उस घोर अंधकारमय की तरह आपातकाल बताने से भी नहीं हिचक रहें है।
आपातकाल तब या आज..
आइए समझने का करें प्रयास-
राष्ट्रीय आपातकाल और अनुच्छेद 352..
भारतीय संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल के प्रावधान को अनुच्छेद 352 के तहत शामिल किया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल को युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण उत्पन्न संकट के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है की आपातकाल केवल तभी घोषित किया जा सकता है जब देश खतरे में हो ना कि किसी के व्यक्तिगत हित के लिए। आपातकाल के दौरान, नागरिकों के मौलिक अधिकार अस्थाई रूप से निलंबित कर दिए जाते हैं। 44वें संशोधन के दौरान, सशस्त्र विद्रोह शब्द को भारत के संविधान में शामिल किया गया था। इससे पहले इसे आंतरिक अशांति के रूप में जाना जाता था।
1975 की एमरजेंसी लगी कैसे.?
भारत में पहला राष्ट्रीय आपातकाल इंदिरा गाँधी की सरकार ने 25 जून 1975 को घोषित किया और यह 21 महीनों तक चला था। इमरजेंसी लगाने का अंतिम निर्णय इंदिरा गांधी लिया गया, जिसे भारत के राष्ट्रपति ने स्वीकार किया। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 को लागू करते हुए देश में आंतरिक गड़बड़ी को आपातकाल घोषित करने का एकमात्र कारण बताते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। इस दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध के साथ-साथ प्रेस पर भी सेंसरशिप लगाई गई।
1975 के आपातकाल के कारण-
एक व्यक्ति कि मजबूत इच्छाशक्ति और आमजन को प्रेरित करने में सिर्फ एक नारा किस तरह से सरकारों के मन में सत्ता खो देने का डर पैदा कर सकता है इसका जीता जागता उदाहरण है “रामधारी सिंह दिनकर” कि ये पंक्तियां “सिंहासन खाली करो कि जनता आती है”। इन पंक्तियों को बुलंद नारे का रूप देकर उपयोग में लेने वाले जयप्रकाश नारायण कि मजबूत इच्छाशक्ति और देश में अपने अधिकारों के लिए जागरूक हुए जनता से इंदिरा गांधी को भी भय लगने लगा। उसी डर के बाद शुरु हुई इमरजेंसी की कहानी..
एमरजेंसी की पहला अध्याय..
इस अध्याय की शुरुआत होती है 1971 के आम चुनावों से जिसमें कांग्रेस को बड़ी जीत मिली थी। उस समय एक नेता थे राजनारायण। जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी से प्रखर समाजवादी नेता थे। इनके इंदिरा गांधी से कई मसलों पर नीतिगत मतभेद थे। इसलिए वे कई बार उनके खिलाफ रायबरेली से चुनाव भी लड़े और हारते रहे। वर्ष 1971 में भी उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन उन्होंने इंदिरा गांधी की इस जीत को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी। यहीं से शुरू हुआ देश में राजनीतिक उथल-पुथल का दौर।
उस समय इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जगमोहन लाल सिन्हा ने अपने फैसले में माना कि इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी और संसाधनों का दुरुपयोग किया है। इसलिए जन-प्रतिनिधित्व कानून के अनुसार उनका सांसद चुना जाना अवैध है। उस समय देश में “इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया” का माहौल था और कोर्ट के फैसले के बाद इंदिरा गांधी के सामने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई जिसमें ना तो वो प्रधानमंत्री बने रह सकती थी और ना ही कोर्ट के आदेश के बाद 6 साल तक चुनाव लड़ सकती थी। तमाम चर्चाओं के बाद इलाहबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट मे चुनौती दी जाती है। इस केस की सुनवाई जज जस्टिस वीआर कृष्णा अय्यर ने की थी। जज ने अपने फैसले में कहा कि वे इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर पूर्ण रोक नहीं लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बने रहने की अनुमति तो दे दी, लेकिन कहा कि वे अंतिम फैसला आने तक सांसद के रूप में मतदान नहीं कर सकती।
दूसरा अध्याय…
एक तरफ क़ानून का शिकंजा कसता जा रहा था वहीं दूसरी और बिहार, गुजरात में कांग्रेस के खिलाफ छात्रों का आंदोलन भी उग्र हो रहा था। बिहार में इस आंदोलन को हवा दे रहे थे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश ने विद्यार्थियों, सैनिकों, और पुलिस वालों से अपील कि वे लोग इस दमनकारी निरंकुश सरकार के आदेशों को ना मानें, क्योंकि कोर्ट ने इंदिरा को प्रधानमन्त्री पद से हटने की बात कह दी थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगले ही दिन यानी 25 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण की रैली थी। जयप्रकाश ने इंदिरा गांधी के ऊपर देश में लोकतंत्र का गला घोंटने का आरोप लगाया और रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता के अंश “सिंहासन खाली करो कि जनता आती है” का नारा बुलंद किया था।
इसी रैली के आधार पर इंदिरा ने अपने खिलाफ बने माहौल को देखते हुए रैली का बहाना बनाकर देश में आपातकाल थोप दिया।
इंदिरा ने 26 जून, 1975 की सुबह राष्ट्र के नाम अपने संदेश में कहा कि जिस तरह का माहौल (सेना, पुलिस और अधिकारियों को भड़काना) देश में एक व्यक्ति अर्थात जयप्रकाश नारायण के द्वारा बनाया गया है। उसमें यह जरूरी हो गया है कि देश में आपातकाल लगाया (National Emergency in India) जाये ताकि देश की एकता और अखंडता की रक्षा की जा सके।
एमरजेंसी 1975.. जब कैद हो गया लोकतंत्र काल कोठरी में-
प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 1975 में सत्ता बचाने के लिए लगाए गए आपातकाल के दौरान एक लाख 10 हजार राजनीतिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी, प्रेस पर सेंसरशिप, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध, संविधान में असंवैधानिक संशोधन, राजनीतिक दलों की गतिविधियों पर पाबंदी लगा दी गयी थी। जनसंख्या विस्फोट को नियंत्रित करने के नाम पर जबरिया नसबंदी और शहरों के सौंदर्यीकरण की आड़ में हजारों गरीबों के घर उजाड़ कर ज्यादतियां की गयी। जाने-माने समाजवादी चिंतक सुरेंद्र मोहन ने अपने एक लेख में लिखा था कि आपातकाल कि घोषणा केवल मौजूदा सरकार, इंदिरा गांधी के निजी फायदों और सत्ता को बचाने के लिए लिया गया फैसला था। इमरजेंसी इंदिरा गांधी और संजय गांधी की तानाशाही का ही नतीजा थी। देश में अव्यवस्था के नाम पर संविधान और कानून में अपने हिसाब से बदलाव किए गए। आपातकाल के पहले हफ्ते में ही संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 22 को समाप्त किया गया। ऐसा कर सरकार ने कानून की नजर में सबकी बराबरी, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी और गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर अदालत के सामने पेश करने के अधिकारों पर रोक लगा दी। अभिव्यक्ति, प्रकाशन करने, संघ बनाने और सभा करने की आजादी को छीनने के लिए जनवरी 1976 में अनुच्छेद 19 को निलंबित किया गया। देशभर में पत्रकारों, मीडिया संस्थानों के मालिकों और संपादकों पर अत्याचार किए गए। यही नहीं कई संपादकों को जेल की हवा तक खिलाई गई। इस दौरान चुन-चुन कर लोगों की नसबंदी कराई गई। दिल्ली साफ सुथरी बनाने के लिए गरीब झुग्गी में रह रहे लोगों के घरों पर बुल्डोजर चलाया गया और लोगों को रातों रात शहर से दूर भेज दिया गया।
वर्तमान सरकार को तानाशाह कहने वाले कुछ राजनीतिक दल और उनसे सबंधित विचारधारा के लोग जब वर्तमान सरकार पर आपातकाल के आरोप लगाते है तो उनको वर्तमान के माहौल को निष्पक्ष रूप से देखने की जरूरत अधिक मालूम पड़ती है। लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार को बेवजह कोसना लोकतंत्र का अपमान है। आरोप लगाने से पहले इन लोगों को समझने की आवश्यकता है की आपातकाल होता क्या है.? और किसने लगाया था.? और आमजन को क्या-क्या झेलना पड़ा था.? आरोप लगाने की बड़ी-बड़ी बातें करने की बजाय बुजुर्गों से चर्चा करके उस समय की परिस्थितियों को समझने की जरूरत है ताकि पता चले की उस समय देश ने क्या-क्या झेला, उस समय आम जनता किस तरह प्रताड़ित की गई, किस तरह उन लोगों ने मजबूत इच्छाशक्ति के दम पर सरकार का सामना किया होगा। निष्पक्ष रूप से परिस्थितियों को देखने पर हम जान पाएंगे की आपातकाल कब था? तब या अब? (ये लेखक के निजी विचार है) एडवोकेट अनिल धायल